
स्पर्श चिकित्सा का परंपरागत इतिहास बुद्ध की किताब में
.jpg) संजय श्रीवास्तव
संजय श्रीवास्तव
इस साल शरीरक्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार प्राचीन ज्ञान को नव्यतम शोध से सत्यापित करता है। यह पुरस्कार इस सर्वकालीन सत्य को भी स्थापित करता है कि छोटी से छोटी, तार्किक, वैज्ञानिक जिज्ञासा बड़ी बड़ी खोजों, आविष्कारों की पूर्वपीठिका बनती है, यह संसार कैसे और बेहतर हो सकता है,हमें इस विमर्श की ओर ले जाती है। यह पुरस्कार एक और बड़ी बात की तरफ इशारा करता है कि बीती सदियों में हम इन दोनों क्षेत्रों में बुरी तरह पिछड़े हैं। न तो हम अपने प्राचीन ज्ञान और तकनीक श्रेष्ठता को अक्षुण्ण और अनवरत रख पाए न ही आधुनिक दौर में तर्कशील वैज्ञानिक सोच समझ वाला जिज्ञासु समाज बना पाये हैं। आध्यात्मिकता, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग के जिन सूत्रों, सिद्धांतों का हमने जिज्ञासापूर्ण वैज्ञानिक, व्यवहारिक आधार और समाधान नहीं ढूंढे, तर्कपूर्ण व्यापक शोध में कोताही बरती, उस क्षेत्र में आज अथक परिश्रम और मेधा के चलते दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने न सिर्फ नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया बल्कि स्थापित सिद्धांतों से चिकित्सा के क्षेत्र में नई आशाएं निर्मित की हैं।
डेविड जूलियस और अर्डेम ने तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स या ग्राही कोशिका या यों कहें कि मानव की त्वचा कोशिकाओं का वह हिस्सा जिससे वह अपने आसपास अथवा संपर्क में आने वाली चीजों का अनुभव करता है, खोज निकाला है। वे अपने अनुसंधान में बताते हैं कि किस तरह हमारा शरीर बाहरी संवेदना को इन रिसेप्टर्स के जरिये ग्रहण करता है और विद्युतीय तरंग में बदल कर उसे संदेश के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जाहिर है इसी से हमें सर्दी गर्मी जलन, चुभन अपने पराये के छूने या दबाने का अहसास होता है। यही अनुभव हमें अपने वातावरण को समझने और उसके प्रति अनुकूलित होने में मदद करते हैं। हमारा शरीर विभिन्न परिवेश और वातावरण में कैसी और क्यों ऐसी प्रतिक्रिया देता है। यह जानना शरीर क्रिया विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में एक चमत्कार साबित हो सकता है। गर्मी, सर्दी या स्पर्श का अनुभव हमारे अस्तित्व के लिये और अपने आसपास के परिवेश के प्रति उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये अनिवार्य तत्व है।
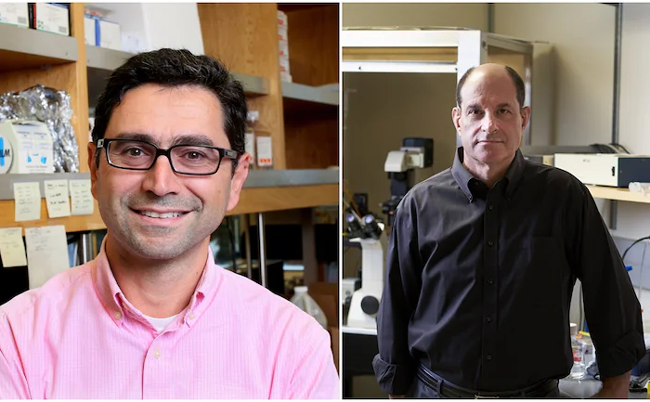
सर्वज्ञात होने के बावजूद अभी तक संज्ञान और वातावरण के बीच इस जटिल रिश्ते और खेल के बीच की यह कड़ी अनसुलझी थी अब प्रोफ़ेसर जूलियस और प्रोफ़ेसर अरडेम पैटापूटियन के प्रयोगों से इन यांत्रिकी उद्दीपकों, प्रेरकों का पता चल गया है। जूलियस ने मिर्च के रसायन कैप्साइनिन से यह समझा कि शरीर किसी जलन या दर्द को प्रसारित कैसे करता है, इसके लिये उन्होंने लाखों डीएनए के अंशों को जांचा जिससे पता लग सके कि कौन सा न्यूरॉन ताप, स्पर्श और दर्द के संवेग को दिमाग तक आगे ले जाता है, जीन की अपनी इस लाइब्रेरी के आधार पर उन्होंने यह जांचा कि गुणसूत्र का वह कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसको इस तरह के प्रोटीन शामिल हैं जो कैप्साइनिन के साथ प्रतिकिया देते हैं। जूलियस ने इसे तलाशा और उस ग्राही हिस्से या रिसेप्टर को उन्होंने टीआरपीवी वन नाम दिया। यह गरमी को पहचानता था तो ठंडक पहचानने वाले रिसेप्टर का नाम दिया टीआरपीएम 8 ।
उधर अरडेम पैटापूटियन ने दबाव या स्पर्श के संवेग अथवा संवेदना को आगे बढाने वाले एक खास रिसेप्टर और उसका आयन चैनल खोज निकाला, इसका नाम उसने ग्रीक भाषा में दबाव के लिये प्रयुक्त पाइजो के नाम पर पाइजो वन और टू रखा। सेल रिपोर्ट्स मेथोड्स की संपादक और ट्रेंडस इन फर्मॉलॉजिकल साइंसेज की पूर्व संपादिका कुसुमिका मुखर्जी कहती हैं कि, यह हमारे इर्दगिर्द के संसार के अनुभव को यह खोज बहुत भीतर तक बदल देगी। मेकेनेसेंसेशन यानी संवेदना के यांत्रिकीकरण में यह अद्भुत खोज बहुत से दर्द की दवा बनेगी। दुनिया का हर पाँचवाँ आदमी किसी न किसी तरह के दर्द से परेशान है। यह शोध निष्कर्ष उन दवा कंपनियों के लिये आशाओं भरा है,जो जटिल दर्द की अकसीर दवा बनाना चाहते हैं। दवा बनाने वाले दर्द के स्रोत और उसके रास्ते का मॉलीक्यूलर या आण्विक स्वभाव और प्रभाव के अनुसार दवा विकसित कर सकेंगे। रसायन या तेज आग से झुलसे लोगों का दर्द इस खोज से मिटाया जा सकेगा। नशे की लत को दूर करने में मदद मिलेगी तो चिकित्सक रक्त वाहिकाओं के दबाव की प्रवृत्ति को बेहतर तरीके से भांप रक्त दिल की बीमारी में दवा को उपयुक्त स्थान तक पहुंचाने का प्रबंध कर सकेंगे।
यह कैंसर, हाइपर टेंशन बेचैनी, तनाव, गठिया, माइग्रेन जैसे कई दर्द और दर्जनों तरह की अन्य बीमारियों के अलावा इम्यून सिस्टम को बेहतर करने, कीमोथिरैपी के साइड इफैक्ट से निबटने, कठिन पीठ दर्द से निजात दिलाने में भी सहायक साबित होगा। एक और बड़ी बात है जिस पर शोध को अगले चरण तक ले जाना होगा वह यह कि शरीर के कोशिका ग्राही हिस्से के बाद स्पर्श या ताप के संवेदी आवेग तंत्रिकातंत्र के जरिये किन अणुओं के माध्यम से वह कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। अब अगर यह रास्ता पता चल गया है तो शीघ्र ही उसकी कार्य प्रकिया समझ कर उसको बाधितकर हम इस तापीय बदलाव के प्रति निस्पृह बन सकते हैं। यदि ऐसा संभव हो सका तो फिर तमाम मौसमी दुष्प्रभावों का, विकट जलवायु परिस्थितियों का मनुष्य पर कोई खास प्रभाव न होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों, व्यवसायों, रोगों के उपचारों के अलावा प्रयोगों परीक्षणों में यह कितना काम आयेगा इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है।
सन 1944 में जोइसेफ इरलेंगर और हरबर्ट गेसेर को इसी क्षेत्र में तकरीबन इसी तरह के खोज के लिये नोबेल मिला था। उन्होंने बताया था कि भिन्न तरह की तंत्रिकाओं के रेशे अलग अलग तरह की उद्दीपन या प्रतिकिया देते हैं जैसे दर्द भरा स्पर्श या सुखद स्पर्श। मतलब यह कि सुख दुःख दर्द और राहत का अहसास कराने वाले तंत्रिकाओं में भेद है। आपकी उंगलियों का एक पोर नम, सूखी, गर्म, चिकनी अथवा खुरदुरी सतह का अनुभव भेद करने में सक्षम हैं। हमें आनंददायक गर्माहट और शदीद गर्मी दोनों का भेद पता चल जाता है। 17वीं शताब्दी में दार्शनिक रैने देकार्ते ने अपने पैर को लपटों के आसपास लाकर महसूस कि यांत्रिक संकेत उस गर्म होती चमड़ी के जरिये ही दिमाग तक पहुंचता है जिसके नीचे बहुत से सूत्र या रेशे छिपे होते हैं। 19वीं सदी में शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा के क्षेत्र के मस्तिष्क के साथ शरीर से संबद्ध जोड़ा गया। इसे बायोफील्ड कहते हैं। इसका असंतुलन रोग और विभिन्न प्रकार की पीड़ा का कारण बताया गया। 1970 में स्पर्श चिकित्सक डोलोरेस क्रेगर ने टच थिरैपी से इसी बायोफील्ड को संतुलित कर बहुत से रोगों और दर्द के इलाज करने का दावा किया। इसे बहुप्रचारित किया। कडलिंग थेरेपी को अपनाकर लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं। रेकी भी कमोबेश इसी सिद्धांत पर काम करता है। हजारों साल पहले भारतीय मनीषियों, योगियों को शरीर के ताप एवं स्पर्श संवेगों को नियंत्रित करने के बारे में भलीभाँति और व्यवहारिक स्तर पर ज्ञान था। तितिक्षा का अभ्यास इसका एक उदाहरण है। अथर्ववेद में स्पर्श चिकित्सा के प्रमाण हैं। ढाई हजार वर्ष पहले बुद्ध की 'कमल सूत्र' नामक किताब में इसका वर्णन बताया जाता है। सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देने से लेकर मालिश तक स्पर्श चिकित्सा का ही हिस्सा है। पर इन सब सैद्धांतिक और किताबी बातों से परे ताज़ा सच यह है कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक शोध का श्रेय जूलियस और अरडम को ही दिया जायेगा जो मानव जीव विज्ञान में अनसुलझे सवाल का मौलिक जवाब फार्मा उद्योग को एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा।